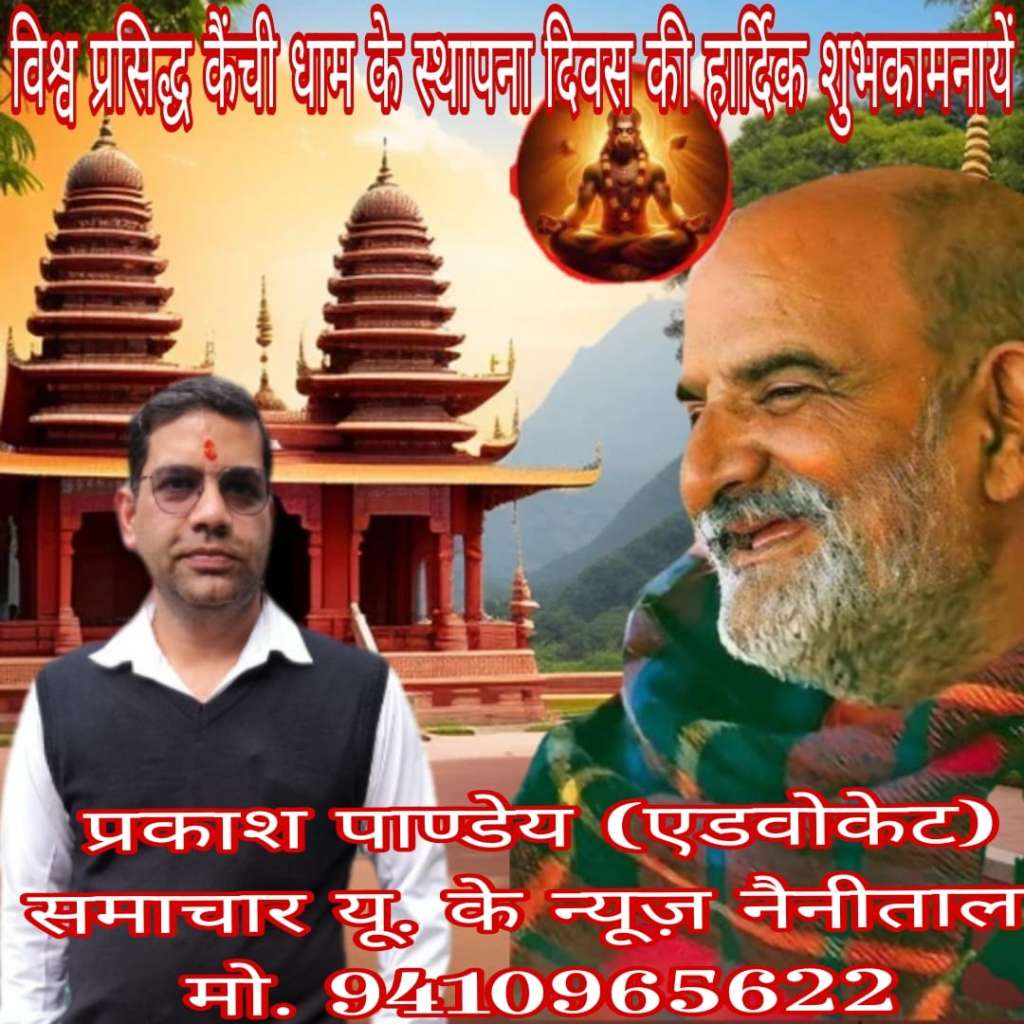बिजली उत्पादन के व्यापार में पर्यावरण की बाज़ी लगाता
बिजली उत्पादन के व्यापार में पर्यावरण की बाज़ी लगाता उत्तराखंड
डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखण्ड राज्य कुल कितनी जल-विद्युत बनाता है उसके पूरे आंकडे उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड के श्रीनगर बांध से कितनी बिजली बनती है, उसका भी ज्ञान नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व वह हिमालस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के पानी से बिजली बनाने के प्रयास में लगा था।
जोशीमठ नगर के 10 किलोमीटर नीचे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा तथा अलकनंदा संगम पर वह 400 किलोवाट बिजली उत्पन्न करता है, जो पूरी-की-पूरी राज्य से बाहर भेजी जाती है, उसका सिर्फ 12 प्रतिशत भाग राज्य के लिए इस्तेमाल होता है। इसे लेजाने-लाने में बहुत सी बिजली व्यर्थ खर्च होती है। अच्छा यह होता कि यह बिजली विष्णुप्रयाग से सीधे उत्तराखंण्ड राज्य को दे दी जाती और फिर बांकी बिजली बाहर भेजी जाती।राज्य की अपनी कितनी बिजली की आवश्यकता है, उसका भी अनुमान नहीं है। राज्य की अधिकतम जल-ऊर्जा बाहर भेजी जाती है इसलिये अपने उपयोग मे बहुत कम ऊर्जा लाई जाती है, नतिजतन राज्य के अधिकतम गांव तथा रास्ते अंधकार में डूबे रहते है। अभी वहां नंदादेवी पर्वत से आने वाले पानी से देश की नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन इस क्षेत्र में जन-विद्युत बनाने का काम कर रही थी। 7 फरवरी को पानी लाने वाली एक हिमानी रेणी गांव के ऊपर टूट गई जिससे नीचे सुरंग में काम कर रहे 250 मजदूर मलबे में दब कर मर गए। कइयों के शरीर अभी भी वहीं पडे हैं और निकाले नहीं गए।उत्तराखण्ड राज्य में ऐसे कोई कारखाने नहीं है, जिसे चलाने के लिए बिजली की आवश्कता हो। यह राज्य कृषि करता है, जिसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। क्योकि राज्य देश की बड़ी-छोटी नदियों का उद्गम स्थल है इसलिए सोचा गया कि क्यों न उनके जल से बिजली बनाई जाय ? इसलिये एक समय उसमें 200 से अधिक जल-विद्युत लाने की योजनाएं बन रही थी।बिजली बनाने का काम सबसे अधिक लाभदायक होता है। बिजली पानी से बनती है, जिसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, खर्चा केवल मशीनों तथा मजदूरों के वेतन पर होता है। जल-विद्युत बनाने में कमाई ही कमाई है। इसलिए यहां जल-विद्युत बनाने हजारों कंपनियां आने का प्रयास करने लगी। कइयों को काम करने के आदेश भी मिल गए फिर खबर उड़ी कि इस काम का ठेका पाने के लिये मंत्री-अधिकारी वर्ग को बहुत धन दिया गया और उस भृष्टाचार के विरुद्ध बहुत प्रतिक्रिया हुई। जिन मंत्री महोदय ने कंपनियों को जल-विद्युत बनाने के परमिट दिए थे उन्होंने उन सब को निरस्त कर दिया और घोटाला शांत हो गया। जल-विद्युत बनाने के काम पर कुछ ही कंपनिया रह गई। पछले वर्षो में राज्य के कितनी बिजली बनाई फिलहाल उसके भी आंकडे नहीं हैं। जितना उत्पादन राज्य का है, उसका कितना भाग बाहर ले जाया और बेचा जाता है उसके भी आंकडे नहीं हैं।यही स्थिति राज्य के अन्य संसाधनों की है। केंद्रीय जल आयोग की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 25 बड़ी जल-विद्युत परियोजनाएं हैं। इनमें से 17 परियोजनाओं से बिजली बन रही है। जबकि 8 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। एनटीपीसी की तपोवन परियोजना भी इनमें से एक थी।इन परियोजनाओं का पर्यावरणीय अध्ययन तो कराया जाता है। लेकिन वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या पर्यावरणीय अध्ययन के लिए सरकार के पास कई संस्थाएं होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिग, वाडिया हिमालयन जियोलॉजी, जीबी पंत इस्टीट्यूट जैसे कई संस्थान हैं जो इस तरह का अध्ययन करते हैं।सभी संस्थाओं की अपनी ख़ास विशेषता है जिसके आधार पर वो अध्ययन करते हैं। जैसे हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट जल प्रवाह से जुड़ा अध्ययन करेगा। आईआईटी की विशेषता इंजीनियरिंग में है। तो जिस संस्था से सरकार को बांधों के पक्ष में रिपोर्ट मिल जाती है उसे मंजूर कर लिया जाता है। जबकि एक जलविद्द्युत परियोजना के लिए नदी का प्रवाह, वहां की भौगोलिक स्थिति, बांध की तकनीकी दक्षता, वहां मौजूद ग्लेशियर की स्थिति जैसे कई पक्षों को देखना होता है।वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक रहे ग्लेशियरोलॉजिस्ट डॉ डीपी डोभाल ने भी यही बात कही। तपोवन परियोजना के पर्यावरणीय अध्ययन में वहां मौजूद ग्लेशियर के बांध पर पड़ने वाले असर का आकलन नहीं किया गया। जबकि यहां तबाही की वजह ग्लेशियर बने।डॉ डोभाल कहते हैं कि बांधों को बनाने से जुड़े पर्यावरणीय अध्ययन में हम उसके ईर्द-गिर्द मौजूद ग्लेशियर का अध्ययन नहीं करते। नदी के जिस पानी के आधार पर हम बिजली बना रहे हैं, वो पानी जिस ग्लेशियर से आ रहा है, उसकी स्थिति समझनी बेहद जरूरी है। डॉ डोभाल आगे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग का असर ग्लेशियर पर भी पड़ रहा है। जिससे ग्लेशियर में बदलाव आ रहे हैं लेकिन उनकी मॉनीटरिंग नहीं हो रही। ग्लेशियर में झीलें बन रही हैं, झीलों की मौजूदा स्थिति क्या है, ग्लेशियर से होने वाला पानी का डिस्चार्ज कितना है, बांधों से जुड़ी परियोजना तैयार करने में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
लेखक द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन उद्यान विभाग के वैज्ञानिक के पद पर का अनुभव प्राप्त हैं, वर्तमान में दून विश्वविद्यालय है.