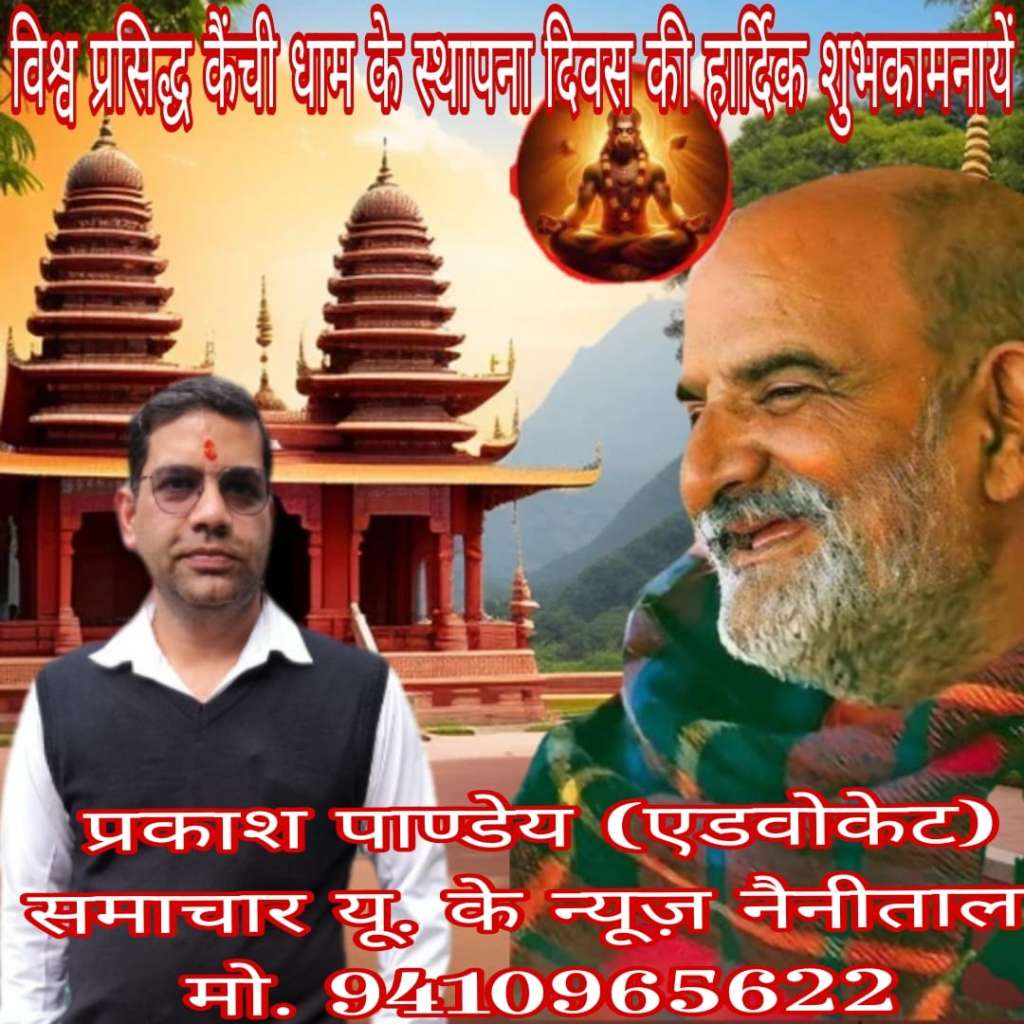वेबिनार के शीर्षक “कला का चहुंमुखी विकास पर ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 सितम्बर 2021 तक


कला का चहुँमुखी विकास (प्रागैतिहासिक से आधुनिक काल तक) – कला की उत्पत्ति मानव के विकास के साथ हुई। सृजन की प्रवृत्ति मानव मन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। इसलिए मानव को समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ट स्थान मिला है। मानव ने अपने जीवन में प्रकृति प्रदत्त साधनों से सदैव जीवन यापन किया है। अपने संघर्षयम जीवन की स्थितियों को संरक्षित रखने के लिए उसने कन्दराओं, शैलाश्रयों एवं गुफाओं में आश्रय लिया। आज इन्हीं स्थानों पर उनके द्वारा रेखांकित आकृतियों से ही हम मानव के इतिहास को कमबद्ध करने का प्रयास करते हैं। मानव मस्तिष्क की चिंतनपरक प्रकिया से विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। मानव के सृजनात्मक कार्य में चित्रकला के साथ अन्य कलाओं के रूपों में भी प्रकृति के साथ संबंध स्थापित हुआ जिसमें सभ्यता का विकास हुआ। मानय के सुसभ्य होने एवं विकासशील प्रवृत्ति से उसके रहन-सहन एवं वेशभूषा से ही उसका इतिहास बना। रहन-सहन की परिवर्तनीय स्थिति से उसे भवनों में आश्रय की प्रेरणा मिली।
भवन निर्माण का कमिक पिकास मानव सभ्यता की ओर सुदृढ़ता प्रदान करता है। सभ्यता के विकास की ओर बढ़ते हुए विभिन्न कालों में वेदों पुराणों उपनिषदों एवं ग्रन्थों की रचना रेखांकनों एवं चित्रों सहित की गयी। मानव जीवन दर्शन में कला संस्कृति के साथ साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में कला संगीत, चित्र, मूर्ति स्थापत्य एवं काव्य का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र में 64 कलाओं के सम्बन्ध में विस्तापूर्वक वर्णन मिलता है। समस्त कलाएँ शिल्पशास्त्र के अन्तर्गत मानी जाती हैं। साहित्य के साथ-साथ कला का विकास विस्तृत रूप से होने लगा, कला आध्यामिक एवं धार्मिक भावनाओं का आश्रय लेकर विकास की ओर बढ़ने लगी। समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार के साथ स्थापत्य एवं शिल्प का अधिक विकास हुआ। सम्राट अशोक द्वारा स्तंभो, स्तूपों एवं भवनों का निर्माण किया गया, बाघ एवं
अजन्ता चित्रों में रेखाओं का भावपूर्ण अंकन एवं रगों के प्रयोग चित्रांकन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गान्धार शैली में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का भी प्रथुरता से निर्माण
किया गया। गुप्तकालीन वास्तुकला में मंदिर निर्माण बड़ी संख्या में हुआ। भारतीय देवी-देवताओं के साथ पुष्प, पशु आकृतियों एवं आलेखनों का अंकन किया गया। राजाओं का संरक्षण पाकर कला का विकास चरम अवस्था पर पहुँच गया। बौद्वकालीन कला में चित्र. मूर्ति एवं स्थापत्य की त्रिवेणी के एक साथ दर्शन होते हैं। असंख्य मठ, विहार और चैत्य बौद्धकला के उज्जवल अतीत के साक्षी हैं। अजन्ता का अनुकरण अनेक शैलियों – पाल, जैन, अपभ्रंश, गुजरात में चित्र निर्माण हुए। इस काल में पोथियाँ ताम्रपत्र पर हैं जिनमें सुन्दर लिपि, तराशे हुए अक्षर और चमकीली स्याही का प्रयोग हुआ है।
18 वीं से 19वीं शताब्दी में गौंड शैली का प्रचलन हुआ जिसमें पदचित्रों के निर्माण की विशेषता रही। पत्चित्रों की परम्परा बंगाल में विषेश रूप से चलती रही। ये चित्र बहुत लोकप्रिय रहे जो आजीविका का सरल साधन बन गये। भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजस्थान के कलाकारों की देन सर्वथा अतुलनीय है। प्राकृतिक सुरम्यता एवं मोहक वातावरण के कारण कला की काव्यमय सृजनशीलता के लिए राजस्थान की धरती बड़ी ही उपयुक्त रही है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजपूत शैली की महत्ता को सरलता से जाना जा सकता है। राजस्थान के प्रत्येक नगरों तथा रजवाड़ों में अपने- अपने ढंग से चित्रकला का सृजन होता रहा है। इसलिए राजपूत शैली में जितनी स्थानीय शैलिओं के दर्शन होते हैं उतने अन्य शैलियों में नहीं भारत में मुगल सल्तनत का अस्तित्व कायम हो जाने के बाद भारतीय कला एवं परम्परागत प्रतिमानों के क्षेत्र में एक प्रबल परिवर्तन हुआ। भारतीय -ईरानी कला ने सामाजिक
एक आद्वितीय, अपूर्व एवं अदभुत युग का सूत्रपात हुआ। बाबर, हुमायूँ. अकबर, जहाँगीर, शाह औरंगजेब के काल तक भारतीय कला, संस्कति एवं समाज का उतार-चढ़ाव चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। मुगल शैली के पतन के उपरान्त पहाड़ी शैली का उत्थान एवं स्वरूप दिखायी देता है। भारतीय परिवेश के चित्रों की एक स्वस्थ परम्परा पहाड़ी शैली के चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। कम्पनी शैली में बंगाल शैली एवं पुनर्जागरण काल में कला का आधुनिक काल एक स्वतन्त्र एवं नवीनतम सृजन के रूप में उजागर हुआ। कला के चहुंमुखी विकास के साथ आर्थिक, सामाजिक , भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक मान्यताओं की प्रेरक स्थितियों पर विचारों को राष्ट्रीय वेबीनार के माध्यम से प्रस्तुत करने के उद्देश्य की पूर्ति होगी। कला का चहुंमुखी विकास के क्रम में समस्त विधाओं पर विचार आंमत्रित हैं।

14 सितम्बर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करा लें। वेबिनार के शीर्षक “कला का चहुंमुखी विकास (प्रागैतिहासिक से आधुनिक काल तक) से सम्बन्धित किसी भी विषय पर अपने विचार अन्तिम तिथि 14 सितम्बर 2021 तक प्रेषित कर सकते हैं। शोध पत्र मेल आई० डी० [email protected] पर pdf फाईल में भेजने का कष्ट करें। वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रतिभाग सम्बन्धित ई-प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
वेबिनार से सम्बन्धित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए नम्बरों पर 11 से 04 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं9411197097, 9719599661, 7818086398, 9084511338