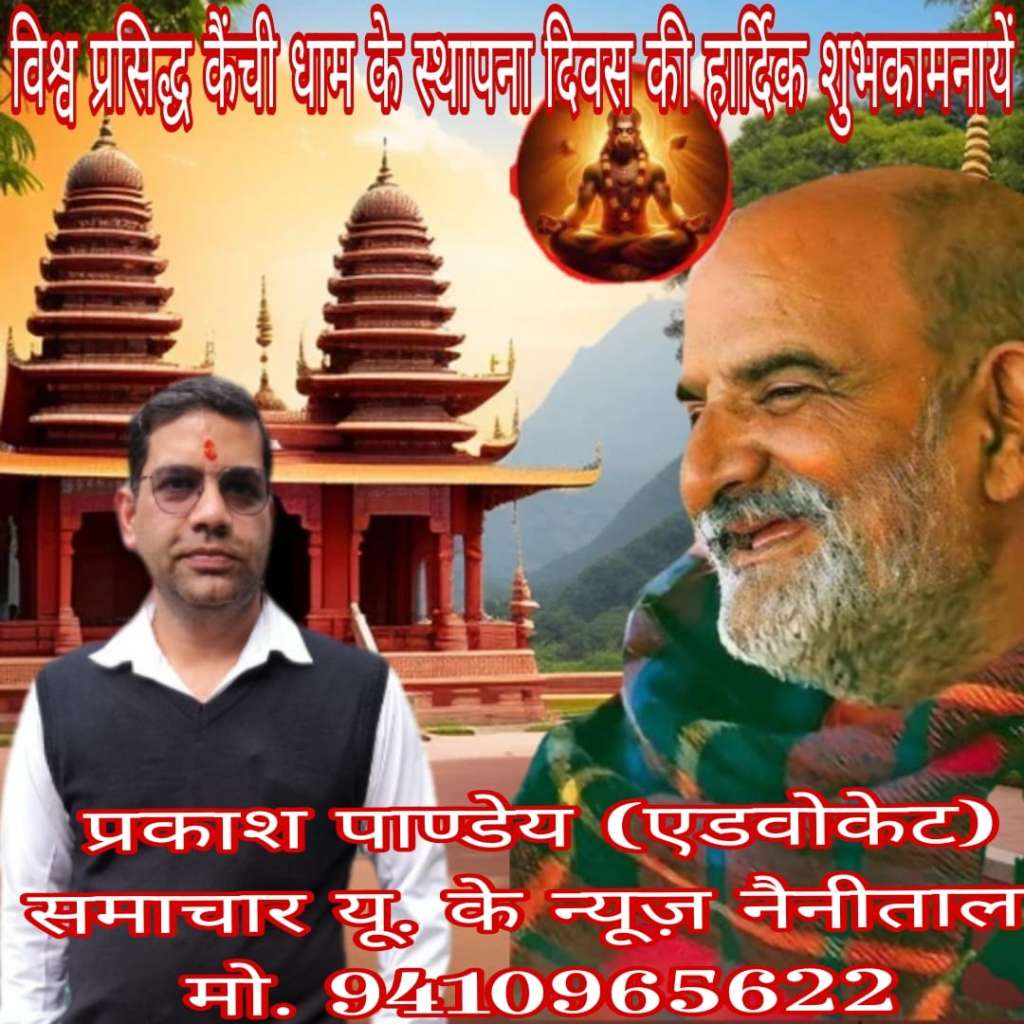गुलदार की आबादी बढ़ने से गुलजार हुए जंगल, माना जाता है धरती का सबसे खतरनाक जीव
गुलदार की आबादी बढ़ने से गुलजार हुए जंगल, माना जाता है धरती का सबसे खतरनाक जीव
डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड
लार्ड डलहौजी के ‘चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट’ 1855 और तदोपरान्त सन् 1864 में इम्पीरियल फारेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना से पूर्व अंग्रेजी शासन की वन या वन्यजीव संरक्षण के प्रति कोई सुनियोजित नीति नहीं थी, इसलिए अपने व्यापारिक हितों की रक्षा तथा स्थानीय समुदाय को हिंसक वन्यजीवों से बचाने के नाम पर बड़े पैमाने पर बाघ एवं तेंदुओं का संहार कराया गया, जिसके लिए तत्कालीन शासन द्वारा परमिट के साथ ही पारितोषिक राशि दिए जाने का भी प्रावधान था। हालांकि पंद्रहवी शताब्दी में मालवा के शासक महमूद खिल्जी ने भी अपने राज्य से बाघ एवं गुलदार जैसे हिंसक वन्यजीवों का उन्मूलन करने का फरमान जारी कर दिया था।कंपनी सरकार के ही कार्यकाल में ब्रिटिश अफसरों द्वारा वन्य जीवों के शिकार के लिए गेम परंपरा भी शुरू की गई। ‘द हिस्टोरिकल जर्नल (वॉल्यूम 58, मार्च 2015) में प्रकाशित विजय रामदास मंडल के शोधपत्र ‘‘द राज एण्ड द पैराडाॅक्स आफ वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन’’ के अनुसार कंपनी सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी में 1822 में 38,483 रुपये पारितोषिक में खर्च कर जनता को बचाने के लिए 5,653 बाघ मरवाए।सन् 1875 में मेजर ट्वीडी ने अपने नोट में कहा था कि हर साल सरकार से इनाम पाने के लिए ब्रिटिश इंडिया में लगभग 20,000 बाघ और गुलदार जैसे हिंसक जीव मरवाए जाते हैं। एक अन्य शोधार्थी रंगराजन के अनुसार सन् 1875 से लेकर 1925 तक ब्रिटिश राज में जनजीवन को बचाने के लिए 80 हजार बाघ और 1.50 लाख गुलदार मारे गए। देश में गुलदारों की संख्या में चार सालों के अंदर 60 प्रतिशत वृद्धि से केंद्र एवं राज्य सरकारों के वन एवं पर्यावरण विभाग गदगद नजर आ रहे हैं। हों भी क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी बिल्ली प्रजाति के बाघ या गुलदार जैसे मांसभक्षी एक स्वस्थ वन्यजीवन और अच्छे पर्यावरण के संकेतक होते हैं। लेकिन गुलदारों के कुनबे में यह उत्साहजनक वृद्धि देश के उन राज्यों में वनों के अंदर और आसपास रहने वाले 27 करोड़ लोगों के लिए खुशी का विषय नहीं बल्कि खतरे का संकेत है, क्योंकि इस धरती पर मानवजीवन के लिए सबसे खतरनाक जीव गुलदार ही माना जाता है।अकेले उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हर साल औसतन 32 लोग वन्यजीवों द्वारा मारे जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक गुलदारों के शिकार होते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गई गणना के आधार पर जारी गुलदारों की नवीनतम संख्या भी केवल सांकेतिक ही मानी जा सकती है, क्योंकि संस्थान ने केवल बाघ संरक्षित क्षेत्रों में यह गणना की है। असली संख्या तो लाखों में होने का अनुमान है।गुलदार निश्चित रूप अन्य मांसहारी जीवों की तरह वन्यजीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। उसे वनों का रखवाला भी कह सकते है। जहां ज्यादा गुलदार या बाघ होंगे वहां निश्चित रूप से उनके निवाले वन्यजीव भी पर्याप्त संख्या में होंगे। वन्य जीवों की पर्याप्त संख्या सघन वनों का ही संकेतक है। लेकिन दूसरी ओर प्रकृति का यह वरदान देश की 27.5 करोड़ की उस आबादी के लिए यमदूत भी है जोकि वनों के अंदर और वनों के आसपास वनों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर हैभारत में हिंसक जीवों में भी गुलदार मनुष्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और असम मानव-गुलदार संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। जिस तरह गुलदार मनुष्य के लिए सबसे खूंखार जीव माना जाता है उसी तरह मानव भी गुलदार के लिए धरती पर सबसे खतरनाक जीव है। वह शिकार सहित ऊंचे-ऊचे पेड़ों पर चढ़ जाता है और पेड़ों के साथ ही आबादी के निकट झाडि़यों में छिपा रहता है। जबकि शेर या बाघ अपने भारी वजन के कारण ने तो पेड़ पर चढ़ सकते है और ना ही आसानी से स्वयं को छिपा सकते।लगातार बढ़ती नरभक्षी गुलदार ( सामान्य बोली में बाघ) के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर अॉक्सफेम इंडिया के माध्यम से किए गए अध्य्यन में यह बात प्रमुख रूप से सामने आई कि नरभक्षी गुलदार या लैपर्ड या बाघ बनने की घटनाएं समान्य नहीं हैं। इनके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं।मांसाहारी जीवों की खाद्यश्रृंख्ला में बढ़ता मानवीय दखल, जिससे जंगल में शाकाहारी जीवों की संख्या घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप मांसाहारी जीव गांवों की ओर या पालतू जीवों की ओर बढ़ रहे हैं।बूढ़े हो चले बाघ और गुलदार, जो गति से भागने वाले हिरन और अन्य जीवों का शिकार नहीं कर पाते, वे गांवों की ओर आकर पहले तो मवेशियों का शिकार करते हैं। और मवेशी के भ्रम में छोटे बच्चों पर भी हमला कर देते हैं।कालांतर में उसी गुलदार या बाघ को छोटे बच्चे आसान शिकार लगते हैं, जिससे वे उनको तलाशने में लगे रहते हैं। गांवों में अधिकतर बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही रह गए हैं, जिससे ये जंगली जानवरों के आसान शिकार माने जाते हैं। 71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में 80 नरभक्षी छुट्टा घूम रहे हैं। इनमें 75 गुलदार और पांच बाघ शामिल हैं। यह कहां हैं, क्या इनकी मौत हो गई, कहीं ये रिवेंज किलिंग (बदले की भावना) का निशाना तो नहीं बने, ऐसे तमाम सवाल भले ही वन्यजीव महकमे के लिए पहेली बने हों, लेकिन इन आदमखोरों का पता न चलने से आमजन के मन से खौफ के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे।वजह यह कि प्रदेश में प्रायः गुलदार और बाघों के हमलों की घटनाएं सुर्खियां बन रही हैं। उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। खासकर गुलदारों ने तो नींद ही उड़ाई हुई है। वन्यजीवों के हमलों की 80 फीसद से अधिक घटनाएं गुलदारों की हैं।मानव के लिए खतरनाक साबित हो रहे गुलदार और बाघों को वन्यजीव महकमा आदमखोर घोषित अवश्य करता है, लेकिन उसकी पहुंच में ये आधे भी नहीं आ पाते। 2006 से अब तक 148 गुलदार और 11 बाघ आदमखोर घोषित किए गए। इनमें सिर्फ 73 गुलदार और छह बाघ ही मारे अथवा पकड़े जा सके।प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष में इस वर्ष अब तक 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले 16 लोगों की जान गुलदार ने ली है। मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव की वजह से नुकसान दोनों को ही हो रहा है। वन महकमा और विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग ने इन घटनाओं को रोकने लिए कुछ प्रयास तो किए हैं, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहे हैं।मानव और वन्यजीवों को जीने के लिए संघर्ष की इस कोशिश में दोनों ही लगातार जान गंवा रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक गुलदार के हमले सामने आ रहे हैं। जनवरी 2021 से चालू माह जुलाई तक अगर 16 लोगों की गुलदार ने जान ली है तो सात गुलदारों को अपनी जान देकर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी।इन्हें मनुष्यों पर हमला करने और जान लेने पर आदमखोर घोषित कर मारा गया। पिछले एक सप्ताह में ही टिहरी और रुद्रप्रयाग में दो गुलदार आदमखोर घोषित कर मारे गए। इन्होंने अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की जान ली थी। वर्ष 2001 से अब तक अलग-अलग कारणों से प्रदेश में 1467 गुलदार की मौत हुई है। इनमें से 72 गुलदार को मनुष्यों पर हमला करने के बाद आदमखोर घोषित कर मारा गया। इस वर्ष चालू माह तक ऐसे सात गुलदारों को मौत के घाट उतारा गया। वर्ष 2021 में अब तक कुल 63 गुलदार की मौत हुई है। इनमें दो गुलदार अज्ञात दुर्घटना में, चार सड़क दुर्घटना में, 14 आपसी संघर्ष में, 17 की स्वभाविक मौत हुई, जबकि 19 गुलदार अज्ञात मौत मरे।वन विभाग की ओर से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा प्रतिफल सामने नहीं आ रहा है। खासकर गुलदार हमलों लगातार तेजी आई है।वन मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि गुलदारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इनकी अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाने के साथ कुछ गुलदार को डीओ कॉलर भी लगाए गए हैं। देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक भी मानव-गुलदार के इस संघर्ष को कम करने के उपायों पर काम कर रहे हैं। मानव और वन्यजीवों को जीने के लिए संघर्ष की इस कोशिश में दोनों ही लगातार जान गंवा रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक गुलदार के हमले सामने आ रहे हैं।हमने गुलदारों पर पूर्व में किए गए शोध के आंकड़ों को विशेषज्ञों के साथ साझा किया है। हमें उम्मीद है कि उनके व्यवहार की बेहतर समझ हमें संघर्ष कम करने के तरीकों में मदद कर सकती है। गुलदार जब भी मानव आबादी में प्रवेश करता है, कुत्ते उसका पहला शिकार होते हैं। खासकर मानसून के सीजन में कुत्ते बारिश और बिजली चमकने के कारण दुबक जाते हैं, ऐसे में गुलदार शिकार न मिलने पर मानवों पर हमला कर देता है। अधिकतर ममालों बच्चे महिलाएं उसके शिकार बनते हैं।भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां अधिकांश मानव आबादी बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। वन निवासियों का दीर्घकाल से वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व रहा है। इसलिए अनिवार्य है कि ऐसी कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाए, जो स्थानीय लोगों की आर्थिक क्षति की पूर्ति कर सके और जन सहभागिता को बढ़ाए ताकि ऐसे भूदृश्य में एकीकृत संरक्षण एवं विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जहां मानव और वन्यजीव साथ-साथ रह सकें।
लेखक द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन उद्यान विभाग के वैज्ञानिक के पद पर का अनुभव प्राप्त हैं, वर्तमान में दून विश्वविद्यालय dk;Zjr है.